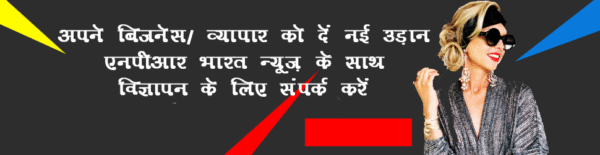लखनऊ : लखनऊ रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, सभी को सचमुच चौंका दिया। लेकिन भीड़ से ज़्यादा चर्चा बसपा के साहस और मायावती की राजनीति, दोनों में झलकती आंतरिक कमज़ोरी की है। पुरानी मायावती सत्ता प्रतिष्ठान को आमने-सामने चुनौती देती थीं, लेकिन अब उसी मंच से भाजपा की तारीफ़ सुनकर उनके अपने कार्यकर्ता स्तब्ध रह गए।
ज़मीनी कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि मायावती 2027 की लड़ाई का ऐलान करेंगी, लेकिन संदेश उल्टा गया और मायावती ने “टकराव की बजाय गतिरोध” का संकेत दिया। हाथी शांत क्यों बैठा है? क्या इसे मायावती का राजनीतिक डर माना जाए या रणनीतिक दूरी? ऐसा लगता है कि मायावती भाजपा का खुलकर सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही हैं। क्योंकि सीबीआई और ईडी की तलवारें, पुराने मुकदमों की यादें और सत्ता के संसाधनों का दबाव शायद अभी भी निर्णायक भूमिका निभा रहा है।
सवाल उठ रहे हैं: दलित आंदोलन और कांशीराम की आत्मा कहाँ गायब हो गई है? बसपा कभी अपने आंदोलन और स्वाभिमान के लिए जानी जाती थी। आज वही संगठन भीड़ तो जुटा सकता है, लेकिन जोश नहीं जगा पाता। नारे वही हैं, बस उनकी धार चली गई है। क्या यह मान लिया जाए कि सामाजिक समीकरण बिखर गए हैं? दलित-मुस्लिम समीकरण बिखर गया है, और युवा मतदाताओं का विश्वास लगातार कम होता जा रहा है? क्या नए मुद्दों पर बसपा की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई है? किसानों, बेरोज़गारी या सामाजिक न्याय पर कोई ठोस रुख़ नहीं?
सवाल यह भी उठता है कि क्या बसपा नेतृत्व का एकालाप और संवादहीनता साफ़ दिखाई दे रही है? दरअसल, आज पार्टी के भीतर संवाद का संकट है। सब कुछ एक व्यक्ति तक सीमित होने से संगठन “विचारहीन और भावशून्य” हो गया है। हालांकि, मायावती की लखनऊ रैली ने एक बात साफ़ कर दी है। हालाँकि यह भीड़ जुटा सकती है, लेकिन जब तक मायावती अपना पुराना रुख़ नहीं अपना लेतीं, तब तक यह कोई भावनात्मक लहर नहीं पैदा करेगी। क्योंकि राजनीति में सम्मान झुकने से नहीं, बल्कि टकराव से मिलता है।